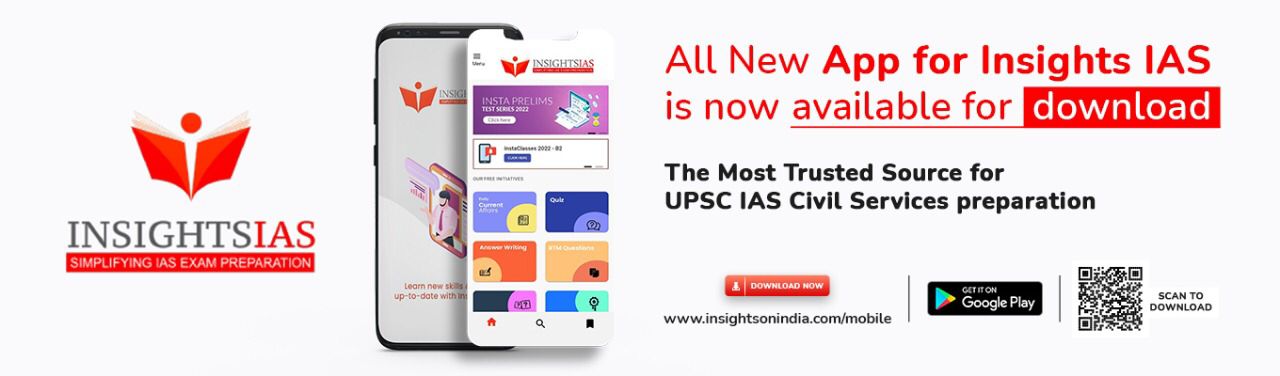[ad_1]
विषयसूची
सामान्य अध्ययन-I
1. महाराजा रणजीत सिंह
2. 1921 का मालाबार विद्रोह
सामान्य अध्ययन-II
1. पीएम-कुसुम योजना
2. कर्नाटक राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण
3. चीन की तीन-बच्चा नीति
सामान्य अध्ययन-III
1. 1989 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एवं किगाली संशोधन
2. ‘ऐतिहासिक’ परमाणु संलयन में सफलता
प्रारम्भिक परीक्षा हेतु तथ्य
1. अफगानिस्तान के हजारा
2. बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना
सामान्य अध्ययन- I
विषय: अठारहवीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास- महत्त्वपूर्ण घटनाएँ, व्यक्तित्व, विषय।
महाराजा रणजीत सिंह
संदर्भ:
हाल ही में, पाकिस्तान स्थित लाहौर के किले में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह की घोड़े पर सवार नौ फुट ऊंची कांस्य निर्मित मूर्ति को तोड़ दिया गया था।
भारत ने इस घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं “खतरनाक दर” से बढ़ती जा रही हैं।
रणजीत सिंह और लाहौर:
- महाराजा रणजीत सिंह (1780-1839) ने, लाहौर के हिंदू,मुस्लिम और सिख अभिजात वर्ग द्वारा शहर पर शासन करने हेतु आमंत्रित किए जाने के बाद वर्ष 1799 में लाहौर को अपने नियंत्रण में लिए लिया था।
- उन्होंने लाहौर में शांति और सुरक्षा स्थापित की और शहर के आर्थिक और सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित किया।
- उन्होंने 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया और सिखों के अलावा अन्य समुदायों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता अपनाते हुए अपने शासन का विस्तार किया।
- उन्होंने बादशाह अकबर द्वारा बनवाए गए लाहौर के किले की मरम्मत भी करवाई थी।
महाराजा रणजीत सिंह के बारे में:
- रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को पंजाब के गुजरांवाला में हुआ था,जो अब पाकिस्तान में है। उस समय,पंजाब पर शक्तिशाली सरदारों का शासन था, और यह क्षेत्र कई मिसलों में विभाजित था।
- रणजीत सिंह ने परस्पर युद्धरत रहने वाली मिसलों को परास्त करके और 1799 में लाहौर पर विजय प्राप्त करने के बाद एक एकीकृत सिख साम्राज्य की स्थापना की।
- महाराजा रणजीत सिंह ने अफ़ग़ानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ीं और उन्हें लाहौर के पश्चिम की ओर खदेड़ दिया। इसके बाद उन्हें ‘पंजाब का शेर’ (शेर-ए-पंजाब) की उपाधि दी गई। लाहौर, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होने तक उनकी राजधानी बनी रहा।
- उनके सेनापति हरि सिंह नलवा ने खैबर दर्रे के मुहाने पर ‘जमरूद के किले’ का निर्माण कराया। इसी मार्ग से विदेशी शासक भारत पर आक्रमण करते थे।
- अपनी मृत्यु के समय, महाराजा रणजीत सिंह भारत में एकमात्र संप्रभु नेता थे, जबकि उस समय तक अन्य सभी राजा किसी न किसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ चुके थे।
प्रशासन:
- महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए बड़ी संख्या में यूरोपीय अधिकारियों,विशेष रूप से फ्रांसीसीयों को तैनात किया था।
- अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए उन्होंने फ्रांसीसी जनरल जीन फ्रैंक्विस एलार्ड को नियुक्त किया था।
- महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य में काबुल और संपूर्ण पेशावर के अलावा मुगलों द्वारा शासित लाहौर और मुल्तान प्रांत शामिल थे। उनके साम्राज्य राज्य की सीमाएँ उत्तर-पूर्व में लद्दाख तक विस्तारित थीं। जम्मू के एक सेनापति जोरावर सिंह ने रणजीत सिंह के नाम पर लद्दाख पर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा, उनका साम्राज्य उत्तर-पश्चिम में खैबर दर्रा और दक्षिण में पंजनाद, जहाँ पंजाब की पाँच नदियाँ सिंधु में मिलती थीं, तक फैला हुआ था।
स्थापत्य योगदान:
- उन्होंने अमृतसर के हरिमन्दिर साहिब गुरूद्वारे में संगमरमर लगवाया और सोना मढ़वाया, तभी से उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा।
- उन्हें महाराष्ट्र के नांदेड़ में, गुरु गोबिंद सिंह के अंतिम विश्राम स्थल ‘हजूर साहिब’ गुरुद्वारे का वित्तपोषण करने का श्रेय भी दिया जाता है।
इंस्टा जिज्ञासु:
क्या आप जानते हैं कि चिल्लियांवाला की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के भारत में अपने पूरे इतिहास के दौरान सबसे ज्यादा अधिकारी मारे गए थे? इस युद्ध के परिणाम क्या रहे?
प्रीलिम्स लिंक:
- महाराजा रणजीत सिंह के बारे में
- उनका प्रशासन
- स्वर्ण मंदिर के बारे में
- लाहौर किले के बारे में
मेंस लिंक:
महाराजा रणजीत सिंह और भारत के आधुनिक इतिहास में उनके योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए।
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस।
विषय: अठारहवीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास- महत्त्वपूर्ण घटनाएँ, व्यक्तित्व, विषय।
1921 का मालाबार विद्रोह
संदर्भ:
20 अगस्त को ‘मालाबार विद्रोह’ के 100 वर्ष पूरे हो रहे है। इस विद्रोह को मोपला (मुस्लिम) दंगों के रूप में भी जाना जाता है।
- ‘मालाबार विद्रोह’ को अक्सर दक्षिणी भारत में हुए पहले राष्ट्रवादी विद्रोहों में से एक माना जाता है।
- इस विद्रोह के दौरान हुए दंगों के कारण मालाबार क्षेत्र में सैकड़ों हिंदुओं की मौत हुई थी, और यह अभी भी इतिहासकारों के बीच एक बहस का विषय बना हुआ है।
मोपला विद्रोह क्या था?
वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह, 19वीं सदी में और 20 वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में, मालाबार क्षेत्र (उत्तरी केरल) में अंग्रेजों और हिंदू जमींदारों के खिलाफ,मोपलाओं (मालाबार के मुसलमानों) द्वारा किये गए विद्रोहों की श्रंखला की एक परिणति थी।
वर्ष 2021 में इस विद्रोह के 100 वर्ष पूरे हो जायेंगे।
विद्रोह के कारण और परिणाम:
ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और सामंती व्यवस्था के खिलाफ आरंभ हुआ यह विद्रोह, अंत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा के रूप में बदल गया।
- मलाबार के निवासियों के बीच असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन के संयुक्त संदेश को फैलाने के लिए, अगस्त 1920 में, गांधीजी तथा भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली ने एक साथ कालीकट का दौरा किया।
- गांधीजी के आह्वान पर, मालाबार में ख़िलाफ़त समिति का गठन किया गया तथा अपने धार्मिक नेता ‘पोंनानी वाले महादुम तंगल’ (Mahadum Tangal of Ponnani) के नेतृत्व में मोपलाओं ने असहयोग आंदोलन में सहयोग करने की शपथ ली।
- इस क्षेत्र में अधिकांश बटाईदारों की समस्याएं, काश्तकारी की सुरक्षा, अत्याधिक लगान, नवीकरण शुल्क (Renewal Fees) तथा जमींदारों द्वारा अन्यायपूर्ण वसूली से संबंधित थीं।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन का कठोरतापूर्वक दमन किया गया तथा इस विद्रोह को कुचलने के लिए गोरखा रेजिमेंटों को लाया गया और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया।
मालगाड़ी त्रासदी (Wagon Tragedy):
ब्रिटिश दमन के दौरान कुछ मोपिला कैदियों को मालगाड़ी से जेल ले जाया रहा था, इसमें से एक डिब्बे में बंद लगभग 60 कैदियों की दम घुट जाने से मौत हो गयी।

इंस्टा जिज्ञासु:
क्या आप ‘वरियामकुननाथ कुंजामहम्मद हाजी’ के बारे में जानते हैं? इनके शासन का अंत किस प्रकार हुआ था:
प्रीलिम्स लिंक:
- वरियामकुननाथ कुंजामहम्मद हाजी’ कौन थे ?
- 1921 में हुए मालाबार विद्रोह के बारे में
- हाजी ने किस प्रकार स्वतंत्र राज्य स्थापित किया?
- खिलाफत आंदोलन क्या है?
- खिलाफत आंदोलन के परिणाम
मेंस लिंक:
वरियामकुननाथ कुंजामहम्मद हाजी कौन थे? वर्ष 1921 में उन्होंने मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार अंग्रेजों का सामना किया? विद्रोह के परिणामों पर चर्चा कीजिए।
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस।
सामान्य अध्ययन- II
विषय: सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।
पीएम-कुसुम योजना
संदर्भ:
हाल ही में, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा ‘प्रधानमंत्री-कुसुम योजना’ (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evem Utthan Mahabhiyan / PM-KUSUM ) के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गयी थी।
समीक्षा के दौरान, किसानों को सिंचाई गतिविधियों के लिए दिन के समय बिजली का विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने के लिए ‘प्रधानमंत्री-कुसुम योजना’ के महत्व पर जोर दिया गया।
प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान / (प्रधानमंत्री-कुसुम योजना) योजना
यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) की एक पहल है।
- इस योजना के तहत, किसानों के लिए देश भर में सौर पंपों और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे।
- फरवरी 2019 में स्वीकृत इस योजना का उद्देश्य वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना है।
- इस योजना का लक्ष्य देश में वर्ष 2022 तक 25,750 मेगावाट सौर ऊर्जा एवं अन्य नवीकरणीय क्षमता की वृद्धि करना है।

योजना के प्रमुख बिंदु:
- ‘प्रधानमंत्री-कुसुम योजना’ के प्रावधानों के अनुसार,ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा युक्त किया जाएगा, इसके लिए केंद्र और राज्य, प्रत्येक द्वारा 30% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और किसान का योगदान 40% रहेगा।
- योजना के तहत फीडर लेवल पर सौरऊर्जा-करण (solarisation) को भी शामिल किया जाएगा।
कार्यान्वयन:
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की राज्य नोडल एजेंसियां ( State Nodal Agencies), योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, डिस्कॉम (Discoms) और किसानों के साथ समन्वय करेंगी।
योजना के लाभ:
- इस योजना से, ग्रामीण भूस्वामियों के लिए उनकी सूखी/ गैर-कृषि योग्य भूमि के उपयोग से 25 वर्ष की अवधि के लिए आय का एक स्थायी और निरंतर स्रोत उपलब्ध होगा।
- यदि सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कृषियोग्य जमीनों को चुना जाता है,तो किसान अपने खेतों में फसल उगाना जारी रख सकते हैं क्योंकि सौर पैनल एक न्यूनतम ऊंचाई से ऊपर स्थापित किए जाएंगे।
- सौर पंपों से, डीजल-चालित पंपों को चलाने के लिए डीजल पर होने वाले खर्च में बचत होगी और डीजल पंपों से होने वाले हानिकारक प्रदूषण को रोका जा सकेगा और इसके अलावा किसानों को सौर पंपों के माध्यम से सिंचाई का एक विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध होगा।
प्रीलिम्स लिंक:
- ‘प्रधानमंत्री-कुसुम योजना’ की मुख्य विशेषताएं
- लाभ
- पात्रता
मेंस लिंक:
‘प्रधानमंत्री-कुसुम योजना’ के महत्व पर चर्चा कीजिए।
स्रोत: पीआईबी।
विषय: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।
कर्नाटक राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण
(Karnataka State Mental Health Authority)
संदर्भ:
कर्नाटक राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन संबंधी प्रक्रिया जारी है।
‘मानसिक स्वास्थ्य’ क्या है?
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार,मानसिक स्वास्थ्य (MENTAL HEALTH) व्यक्ति के स्वास्थ्य की एक स्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने, जीवन में आने वाले सामान्य तनावों का सामना करने, लाभकारी ढंग से काम करने और अपने समुदाय में भागीदारी करने में सक्षम होता है।
मानसिक स्वास्थ्य के निर्धारक:

वर्तमान में ‘मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण’ की आवश्यकता:
कोविड- 19 महामारी के बाद ‘साधारण’ लोगों के ‘असाधारण स्थितियों’ के संपर्क में आने से ‘मानसिक स्वास्थ्य’ संबंधी मामले बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं।
- ऐसे मामले विविध रूपों में सामने आ रहे हैं, जिनमें चिंता, अवसाद जैसी भावनात्मक तकलीफें और अनिद्रा, भूख में कमी जैसे जैविक प्रभाव तथा मादक द्रव्यों का सेवन और सदमे से उभरने के बाद होने वाली व्यथाएं आदि शामिल हैं।
- महिलाओं,बच्चों और बुजुर्गों जैसे संवेदनशील लोगों के लिए, घरेलू हिंसा, सामाजिक अलगाव, स्क्रीन समय में वृद्धि और गरीबी का सामना करने जैसी अधिक जटिल चुनौतियों ने उनके मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर उल्लेखनीय तथ्य:
विश्व स्वास्थ्य संगठन (2020) के अनुसार:
- विश्व स्तर पर भारत में 36.6 प्रतिशत आत्महत्याएं होती हैं।
- लगभग 7.5 प्रतिशत भारतीय किसी न किसी मानसिक विकार से पीड़ित हैं और 2020 के अंत तक इस संख्या में लगभग 20 प्रतिशत तक वृद्धि होने की संभावना है।
- गणना के अनुसार, 56 मिलियन भारतीय अवसाद से पीड़ित हैं और अन्य 38 मिलियन भारतीय चिंता-विकारों से ग्रस्त हैं।
- विकलांगता समायोजित जीवन वर्षों (Disability adjusted life year – DALYs) के संदर्भ में, भारत में कुल बीमारियों के भार में मानसिक विकारों का योगदान वर्ष 1990 में 5% से बढ़कर वर्ष 2017 में 4.7% हो गया था।
- भारत में, प्रति 100,000 की आबादी पर मनोचिकित्सक (0.3), नर्स (0.12), मनोवैज्ञानिक (0.07) और सामाजिक कार्यकर्ता (0.07) हैं, जबकि वांछनीय संख्या प्रति 100,000 की आबादी पर मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों की संख्या तीन से अधिक है।
मानसिक स्वास्थ्य संबंधी संवैधानिक और विधिक अधिदेश:
- अनुच्छेद 21– ‘गरिमामय जीवन का अधिकार’ के विस्तार में ‘मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने का अधिकार’ भी शामिल है। इसको ‘मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम’ 2017 (Mental Healthcare Act, 2017) के तहत ‘गरिमामय जीवन का अधिकार’ के रूप में मान्यता प्रदान की गयी थी।
- अनुच्छेद 47– ‘पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊँचा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना’ राज्य का कर्तव्य होगा।
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दोहराया है, कि मानसिक बीमारी वाले प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार होगा।
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017:
- प्राधिकरण का गठन– केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण।
- बोर्ड का गठन: राज्य प्राधिकरण द्वारा ‘मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का गठन।
- आत्महत्या का गैर-अपराधीकरण – आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को उस समय मानसिक बीमारी से पीड़ित माना जाएगा और उसे भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित नहीं किया जाएगा।
- विद्युत्-आक्षेपी चिकित्सा (Electroconvulsive therapy / ECT) या शॉक थेरेपी का निषेध- मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाओं और एनेस्थीसिया के साथ ही इलेक्ट्रो-कंवल्सिव थेरेपी दी जा सकती है। नाबालिगों के लिए यह थेरेपी निषिद्ध है।
- अग्रिम निर्देश- यह अधिनियम, मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को ‘अग्रिम निर्देश’ (advance directive) देने का अधिकार दिया गया है, जिसमे व्यक्ति, अपनी बीमारी का इलाज किस प्रकार कराना चाहता है, यह बता सकता है।
- बीमा: अधिनियम में कहा गया है, कि प्रत्येक बीमाकर्ता मानसिक बीमारी के इलाज के लिए उसी आधार पर चिकित्सा बीमा का प्रावधान करेगा जो शारीरिक बीमारी के इलाज के लिए उपलब्ध है।
मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार:
- प्रत्येक व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार।
- मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में गोपनीयता का अधिकार।
आवश्यकता:
- समग्र स्वास्थ्य बजट में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय के अनुपात में वृद्धि की जाए।
- प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या में वृद्धि की जाए।
- ‘स्वच्छ मनसिकता अभियान’जैसे अभियानों के माध्यम से मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक से निपटने के लिए व्यापक जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ायी जाए।

इंस्टा जिज्ञासु:
जुलाई 2018 में लागू हुए ‘मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम’ (MHCA),2017, ने आईपीसी की धारा 309 के उपयोग की गुंजाइश को काफी कम कर दिया है। धारा 309 क्या है?
प्रीलिम्स लिंक:
- IPC की धारा 309 के अंतर्गत किसे अपराधी घोषित किया जा सकता है?
- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम (MHCA), 2017 के प्रमुख प्रावधान
- विधि आयोग- संविधान और रचना
- MHCA की धारा 115 (1)
मेंस लिंक:
हाल के वर्षों में, आत्महत्या संबंधी मामलों ने चिंताजनक रूप से ध्यान आकर्षित किया है। भारत में उच्च आत्महत्या मृत्यु दर के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा भारत इस चुनौती का सामना किस प्रकार कर है?
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस।
विषय: भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव; प्रवासी भारतीय।
चीन की तीन-बच्चा नीति
(China’s three-child policy)
संदर्भ:
चीन की विधायिका द्वारा दम्पतियों को तीन बच्चे पैदा करने की अनुमति देने हेतु देश के परिवार नियोजन नियमों में औपचारिक रूप से संशोधन किया गया है,साथ ही घटती जन्म दर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नीतिगत उपायों की घोषणा की गयी है।
इन निर्णयों के पीछे कारण:
- हाल ही में जारी किए गए,चीन में की गयी दशकीय जनगणना आंकड़ों से पता चला है, कि देश की जनसंख्या वृद्धि दर,तेजी से घटती जा रही है।
- चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, पिछले साल 12 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ,जोकि 1961 के बाद सबसे कम है।
चीन में ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ क्यों लागू की गई थी?
- चीन द्वारा ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ की शुरुआत वर्ष 1980 में की गई थी, उस समय चीन की जनसँख्या लगभग एक अरब के करीब पहुंच रही थी और कम्युनिस्ट पार्टी को इस बात की चिंता थी कि देश की बढ़ती आबादी, आर्थिक प्रगति को बाधित करेगी।
- इस नीति को लागू करने के लिए कई तरीके अपनाए गए थे, जिनके तहत, एक बच्चा पैदा करने वाले परिवारों के लिए आर्थिक रूप से प्रोत्साहन, गर्भनिरोधकों को व्यापक रूप से उपलब्ध कराना और नीति का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रतिबंध लगाना, आदि शामिल थे।
इस नीति की आलोचनाएँ:
चीनी अधिकारियों द्वारा लंबे समय तक इस नीति को एक सफलता के रूप में बताया जाता रहा, और दावा किया गया कि, इस नीति ने, लगभग 40 करोड़ लोगों को पैदा होने से रोक कर देश के समक्ष आने वाली भोजन और पानी की कमी संबंधी गंभीर समस्याओं को टालने में मदद की है।
हालाँकि, एक बच्चे पैदा करने की सीमा, देश में असंतोष का एक कारण भी थी, जैसेकि:
- इसके लिए, राज्य द्वारा जबरन गर्भपात और नसबंदी जैसी क्रूर रणनीति का इस्तेमाल किया गया।
- यह नीति, गरीब चीनियों के लिए काफी अन्यायपूर्ण थी, क्योंकि अमीर लोग, नीति का उल्लंघन करने पर आर्थिक प्रतिबंधों का भुगतान कर सकते थे और गरीबों को दंड भुगतना पड़ता था।
- इस नीति को लागू करने के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया।
- इसने सामाजिक नियंत्रण करने के एक उपकरण के रूप में, प्रजनन सीमाओं को लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया।
- इसने पुरुषों के पक्ष में लिंगानुपात को प्रभावित किया।
- इसकी वजह से कन्या भ्रूणों के गर्भपात में वृद्धि हुई और इसी तरह अनाथालयों में परित्यक्त लड़कियों की संख्या बढ़ी।
- इसकी वजह से चीन में वृद्धो की संख्या में अन्य देशों की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई, जिससे देश की विकास क्षमता प्रभावित हुई।
इस नीति को क्यों बंद कर दिया गया?
तेजी से बढ़ती वृद्ध आबादी की वजह से आर्थिक विकास को नुकसान पहुचने के भय से सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक-बच्चा नीति’ (One-Child Policy) में बदलाव कर प्रत्येक विवाहित जोड़े को दो बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई।
आगे के सुधारों की क्या आवश्यकता थी?
हालांकि, ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ में छूट देने से देश में युवा लोगों के अनुपात में कुछ सुधार तो हुआ किंतु इस नीति परिवर्तन के लिए ‘आसन्न जनसांख्यिकीय संकट’ को टालने हेतु अपर्याप्त माना गया।
आगे की चुनौतियां:
विशेषज्ञों का कहना है. कि केवल प्रजनन अधिकारों पर ढील देने से आगामी अवांछित जनसांख्यिकीय बदलाव से बचने में बहुत मदद नहीं मिल सकती है।
वर्तमान में कम बच्चे पैदा होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
- जीवन यापन, शिक्षा और वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण की बढ़ती लागत
- देश में लंबे समय तक काम करने की संस्कृति
- कई दम्पतियों का मानना है कि एक बच्चा काफी है, और वे अतिरिक्त बच्चे पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।
चीन की नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के बारे में जानने हेतु: Puucho करेंट अफेयर्स+ पीआईबी नोट्स [ DAILY CURRENT AFFAIRS + PIB Summary in HINDI ] 12 May 2021 – IASPuucho (insightsonindia.com)
इंस्टा जिज्ञासु:
उत्तर प्रदेश की दो बच्चा नीति का संक्षिप्त विवरण प्राप्त करें।
प्रीलिम्स लिंक
- चीन में ‘एक बच्चे की नीति’ क्या है?
- भारत में परिवार नियोजन
- इस संबंध में सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाएं और नीतियां
मेंस लिंक:
‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कीजिए।
स्रोत: द हिंदू।
सामान्य अध्ययन- III
विषय: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।
1989 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एवं किगाली संशोधन
संदर्भ:
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए ‘किगाली संशोधन’ (Kigali Amendment) के अनुसमर्थन को स्वीकृति दी है।
‘किगाली संशोधन’ क्या है?
- इस संशोधन को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए अक्टूबर, 2016 में रवांडा की राजधानी ‘किगाली’ में आयोजित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 28 वीं बैठक के दौरान अंगीकृत किया गया था।
- यह संशोधन पहले ही वर्ष 2019 की शुरुआत से लागू हो चुका है।
- ‘किगाली संशोधन’ के तहत, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs), एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन और फर्निशिंग फोम उद्योग में बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने वाले रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु प्रावधान किए गए हैं।
किगाली संशोधन के तहत निर्धारित लक्ष्य:
- इस सदी के मध्य से पहले, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के वर्तमान उपयोग को कम से कम 85 प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशों द्वारा अलग-अलग समय-सीमाएं निर्धारित की गयी है।
- भारत के लिए यह लक्ष्य वर्ष 2047 तक हासिल करना है जबकि विकसित देशों के लिए वर्ष 2036 तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी है। चीन और कुछ अन्य देशों के लिए यह समय-सीमा वर्ष 2045 तय की गयी है।
- समृद्ध देशों द्वारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन में कटौती तत्काल तुरंत शुरू की जानी चाहिए। भारत और कुछ अन्य देशों को अपने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उपयोग में वर्ष 2031 से कटौती शुरू करनी होगी।
महत्व और अपेक्षित परिणाम:
- यदि किगाली संशोधन के प्रावधानों को सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो इससे, सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग में होने वाली वृद्धि को लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सकता है।
- प्र्सतावित लाभों की दृष्टि से और कार्यान्वयन में आसानी के मामले में, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए लागू किया गया कोई भी एकल हस्तक्षेप, ‘किगाली संशोधन’ के प्रावधानों के करीब भी नहीं आता है।
- अतः पेरिस समझौते में निर्धारित ‘पूर्व-औद्योगिक समय से 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर तापमान वृद्धि को प्रतिबंधित’ करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
‘हाइड्रोफ्लोरोकार्बन’ क्या हैं?
- ग्लोबल वार्मिंग / वैश्विक उष्मन के कारणों के रूप में ‘हाइड्रोफ्लोरोकार्बन’ (Hydrofluorocarbons – HFCs) को ‘कार्बन डाइऑक्साइड’ से भी बदतर माना जाता है।
- वास्तव में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अनुसार, सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले 22 ‘हाइड्रोफ्लोरोकार्बन’ की औसत ग्लोबल वार्मिंग क्षमता, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 2,500 गुना अधिक होती है।
‘मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल’ के बारे में:
- वर्ष 1989 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol) का उद्देश्य ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत की सुरक्षा करना है।
- इस प्रोटोकॉल के तहत, क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) और अन्य ओजोन-क्षयकारी पदार्थों (ozone-depleting substances – ODS) के पूर्णतयः हटाने को अनिवार्य किया गया है। पिछले तीन दशकों से यह प्रोटोकॉल अपने प्रावधानों को सफलतापूर्वक लागू करने में कामयाब भी रहा है।
वर्तमान चिंताएं:
- क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) को धीरे-धीरे ‘हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन’ (Hydrochlorofluorocarbons HCFCs) से परिवर्तित किया जा रहा है, और कुछ मामलों में, इसकी जगह ‘हाइड्रोफ्लोरोकार्बन’ (HFCs) लेता जा रहा है, जिसका ओजोन परत पर अपेक्षाकृत न्यूनतम प्रभाव पड़ता है।
- ‘हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन’ की जगह ‘हाइड्रोफ्लोरोकार्बन’ में परिवर्तन अभी भी कई देशों में, खासकर विकासशील देशों में जारी है।
- ‘हाइड्रोफ्लोरोकार्बन’, हालांकि ओजोन परत के लिए कम हानिकारक होती है, किंतु फिर भी यह काफी शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें होती है।
- यदि इन गैसों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में इनका योगदान वर्ष 2050 तक 19% तक पहुंच सकता है।
इंस्टा जिज्ञासु:
क्या आप जानते हैं कि 2019 में जारी बीस वर्षीय ‘इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान’ (India Cooling Action Plan – ICAP) में ‘कूलिंग’ को “विकासात्मक आवश्यकता” के रूप में वर्णित किया गया है? आईसीएपी के बारे में अधिक जानने हेतु पढ़ें।
प्रीलिम्स लिंक:
- किगाली संशोधन के बारे में
- लक्ष्य
- ‘हाइड्रोफ्लोरोकार्बन’ (HFCs) बनाम ‘हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन’ (HCFCs)
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में
- अन्य ओजोन-क्षयकारी पदार्थों (ODS) के बारे में
मेंस लिंक:
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस।
विषय: सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता।
‘ऐतिहासिक‘ परमाणु संलयन में सफलता
(‘Historic’ Nuclear Fusion Breakthrough)
संदर्भ:
कैलिफ़ोर्निया के भौतिकविदों ने फ़ुटबॉल के तीन मैदानों के आकार के लेज़रों का उपयोग करके संलयन के माध्यम से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है।
इस सफलता के बाद एक नए स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के विकास की आशा दिखाई देती है।
प्रयोग का क्रियान्वयन एवं परिणाम:
- विशेषज्ञों द्वारा, पहले की तुलना में आठ गुना अधिक ऊर्जा का महा-विस्फोट निर्मित करने के लगभग 200 लेजर बीम की अपनी विशाल श्रंखला को एक छोटे से स्थान पर केंद्रित किया गया।
- हालांकि, प्रयोग में उत्पन्न ऊर्जा अत्याल्प समय – एक सेकंड के सिर्फ 100 ट्रिलियनवें हिस्से – के लिए उत्पन्न की जा सकी, किंतु वैज्ञानिक जितनी उर्जा का उपयोग कर रहे थे, उससे कहीं अधिक ऊर्जा पैदा करने में सक्षम थे।
इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन के दो समस्थानिकों का प्रयोग किया था, जिससे विशाल मात्रा में हीलियम उत्पन्न हुई।
संलयन क्या होता है और यह विखंडन से किस प्रकार भिन्न होता है?
- ‘परमाणु संलयन’ (Nuclear fusion) प्रक्रिया में बहुत कम अपशिष्ट उत्पन्न होता है और इसमें किसी ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन भी नहीं होता है, इसीलिये, इसे कुछ वैज्ञानिकों द्वारा भविष्य की संभावित ऊर्जा माना जाता है।
- संलयन (Fusion), वर्तमान में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक ‘परमाणु विखंडन’ (Nuclear fission) से भिन्न होती है। ‘विखंडन’(fission) प्रक्रिया में भारी परमाणु नाभिक के बंध टूट कर ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं।
- संलयन (Fusion), सूर्य तथा अन्य तारों का ऊर्जा स्रोत है। इन तारकीय निकायों के केंद्र में अत्याधिक ऊष्मा तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण, हाइड्रोजन नाभिक परस्पर टकराते हैं, इसके परिणामस्वरूप हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर भारी हीलियम अणुओं का निर्माण करते हैं जिससे इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती हैं।
इंस्टा जिज्ञासु:
क्या आप चीन के ‘कृत्रिम सूर्य’ प्रायोगिक संलयन रिएक्टर के बारे में जानते हैं?
प्रीलिम्स लिंक:
- परमाणु संलयन बनाम परमाणु विखंडन
- संलयन और विखंडन के उपोत्पाद
- सूर्य की ‘कोर’ के बारे में
- अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (ITER) क्या है?
मेंस लिंक:
चीन द्वारा विकसित किए जा रहे कृत्रिम सूर्य के महत्व का वर्णन कीजिए।
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस।
प्रारम्भिक परीक्षा हेतु तथ्य
अफगानिस्तान के हजारा
‘हजारा’ (Hazara) अफगानिस्तान का एक जातीय समूह है।
- ये मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान के वंशज माने जाते है थे, चंगेज खान और उसकी सेना ने 13 वीं शताब्दी के दौरान पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था।
- उनकी विशिष्ट एशियाई शारीरिक लक्षण और हजारगी नामक फ़ारसी बोली का उपयोग भी उन्हें देश के बाकी हिस्सों से अलग करता है।
बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना
- हाल ही में, ओडिशा सरकार द्वारा ‘बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना’ (Biju Swasthya Kalyan Yojana – BSKY) स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की गयी है।
- इस योजना के तहत, राज्य के लगभग 96 लाख परिवारों के लिए 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्रदान की जाएगी। BSKY के तहत महिला लाभार्थियों के लिए खर्च की सीमा 10 लाख रुपये है।
- स्मार्ट कार्ड धारकों को राज्य के 200 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस स्वास्थ्य बीमा लाभ भी प्राप्त होगा।
Join our Official Telegram Channel HERE for Motivation and Fast Updates
Subscribe to our YouTube Channel HERE to watch Motivational and New analysis videos
[ad_2]